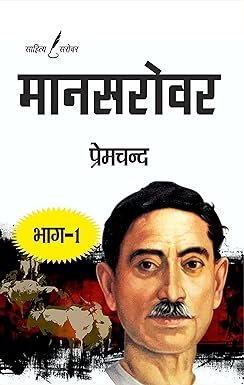‘मानसरोवर – 1: मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानियों का सारांश और रिव्यू’।
मानसरोवर – 1
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित
रिव्यू –
लेखक की जानकारी –
महान हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद इन्होंने उपन्यासों के साथ – साथ कई कहानियाँ भी लिखी | उन्ही कहानियों के विशाल संग्रह को उनके निधन के बाद आठ खंडों में प्रकाशित किया गया | मानसरोवर – भाग १ इसी सीरीज का पहला भाग है | लेखक मुंशी प्रेमचंद को ‘उपन्यास सम्राट’ के नाम से भी जाना जाता है |
वह आधुनिक हिंदी तथा उर्दू साहित्य के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं | मानसरोवर के पहले भाग मे 23 कहानियाँ संकलित की गई है | प्रस्तुत कहानियाँ मूल रूप से हिंदी और उर्दू भाषा के मिश्रण में लिखी गईं थी लेकिन वर्तमान समय मे इसे मुख्य रूप से हिंदी में प्रकाशित किया जाता है |
प्रेमचंद की कहानियाँ सामाजिक यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध हैं | यह संग्रह उस समय के भारतीय जीवन, विशेषकर ग्रामीण भारत के लोगों के संघर्षों, भावनाओं और आकांक्षाओं का सजीव चित्रण करता है |
उपन्यास की कहानियाँ –
‘मानसरोवर – 1’ की कहानियाँ समाज और मानवीय जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं | कहानियों में गरीबी, जातिवाद, वर्ग-भेदभाव और जमींदारी व्यवस्था के कारण किसानों के शोषण को प्रमुखता से दर्शाया गया है | ये कहानियाँ साधारण लोगों की नैतिकता, दया, त्याग, संघर्ष और धैर्य जैसी मानवीय भावनाओं को कुशलता से उजागर करती हैं |
इसमें समाज में विधवाओं की स्थिति, दहेज प्रथा और पुरुषप्रधान समाज में महिलाओं की चुनौतियों पर भी गंभीर चित्रण मिलता है |
इस खंड में प्रेमचंदजी की कुछ सबसे प्रसिद्ध कहानियाँ शामिल हैं | जिनके नाम है – ईदगाह , बड़े भाई साहब , पूस की रात , ठाकुर का कुआँ , घासवाली , नशा , अलग्योझा | इसमे से हम “बड़े भाई साहब” कहानी के बारे मे “शतरंज के खिलाड़ी” मे बात कर चुके है | उस ब्लॉग को भी आप एक बार जरूर चेक करे |
Check out our other blog post SHATRANJ KE KHILADI
पुस्तक हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, जो पाठकों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई के साथ जोड़ती है | हमारी तरफ से इस किताब को 5 स्टार की रेटिंग है | आज के इस ब्लॉग मे हम , ” ईदगाह , ‘पूस की रात’ ,ठाकुर का कुआँ’ गुल्ली-डंडा’ इन कहानियों के बारे मे बात करेंगे | इसलिए सारांश भी इन्ही का देखेंगे | प्रस्तुत किताब के –
लेखक है – मुंशी प्रेमचंद
प्रकाशक है – साहित्य सरोवर
पृष्ठ संख्या – 350
उपलब्ध – अमेजन पर
सारांश –
‘ईदगाह’ – कहानी का सारांश
मुंशी प्रेमचंद की सबसे भावुक और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानियों में से एक है | यह बाल-मनोविज्ञान, गरीबी के प्रभाव और मातृ-पितृ स्नेह को गहराई से दर्शाती है | इसीलिए शायद इसे बच्चों के पाठ्यक्रमों मे शामिल किया गया होगा ताकि बच्चे भी इस कहानी से कुछ सिख सके | वह भी अपने बड़े – बुजुर्गों के प्रति प्रेम , आदर , सम्मान रख सके |
हामिद एक चार-पाँच साल का अनाथ, गरीब और समझदार बच्चा है | वही इस कहानी का नायक है | अमीना , हामिद की बूढ़ी और गरीब दादी है | वही उसके जीवन का एकमात्र सहारा है | महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी यह हामिद की मित्रमंडली है | कहानी रमज़ान के पूरे तीस रोज़ों के बाद आए ईद के दिन से शुरू होती है | पूरे गाँव में ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ने और मेला घूमने का उत्साह है | हामिद अत्यंत गरीब है |
गरीबी के बावजूद वह खुश है क्योंकि उसकी दादी ने उसे बताया है कि उसके पिता ढेर सारा पैसा कमाने गए हैं और माँ अल्लाह के घर से उसके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने गई हैं |
हामिद के पास मेले में खर्च करने के लिए केवल तीन पैसे हैं, जबकि उसके दोस्तों के पास ज़्यादा पैसे हैं | ईदगाह तक बच्चों का सफर बड़े मजे मे कटता है | ईदगाह पहुँचकर नमाज़ के बाद मेला शुरू होता है | मेले में घूमते हुए, हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है जबकी उसके दोस्त मिट्टी के अलग -अलग खिलौने खरीदने मे व्यस्त है |
वह सोचता है कि उसकी दादी अमीना जब भी तवे पर रोटी बनाती है, तो उसकी उँगलियाँ जल जाती हैं | हामिद अपने मन पर काबू रखकर अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करता है क्योंकि उसके पास सिर्फ तीन पैसे है |
वह इससे एक तो खिलौने खरीद सकता है या फिर अपनी दादी के लिए चिमटा | वह चिमटा चुनता है | खुद की इच्छाओ को मारकर अपनी दादी को सुख देना चाहता है |
घर आने के बाद , सारी कहानी जानकर अमीना के आँखों से आँसू बहने लगते हैं | वह हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर अभिभूत हो जाती है | प्रेमचंद यहाँ कहते हैं कि “बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है!” इस क्षण, बूढ़ी अमीना बालिका बन जाती है, और चार साल का हामिद बूढ़ा | कहानी दर्शाती है कि गरीबी और अभाव एक बच्चे को उसकी उम्र से पहले ही बड़ों जैसा समझदार और ज़िम्मेदार बना देते हैं |
दूसरी कहानी है – “पूस की रात” कहानी का सारांश |
“पौष” महीने को देहाती भाषा मे “पूस” कहा जाता है | मराठी पंचांग के अनुसार पौष महिना आमतौर पर दिसंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक आता है | इन दिनों काफी ठंड पड़ती है | इसी ठंड मे एक किसान की हालत क्या होती है जो रात को खेतों की रखवाली करता है | यह कहानी उसी पर प्रकाश डालती है |
प्रस्तुत कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है, जो भारतीय किसान के शोषण, कर्ज और लाचारी को दर्शाती है | | यह कहानी 1930 में प्रकाशित हुई थी |
हल्कू एक गरीब, अभावग्रस्त किसान है जो साहूकार के कर्ज तले दबा हुआ है | मुन्नी , उसकी पत्नी है जो घर के खर्चों में कटौती करके उस के लिए एक कंबल खरीदने की कोशिश करती है |
हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से वह तीन रुपये माँगता है, जो मुन्नी ने बड़ी मुश्किल से पूस की ठंड से बचने के लिए हल्कू के लिए एक कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे | यही पैसे हल्कू साहूकार को देना चाहता है क्योंकि साहूकार उसपर पैसों के लिए दबाव डाल रहा है | हल्कू साहूकार की गालियाँ सुनने से बचने के लिए मन मारकर वह पैसे साहूकार को दे देता है |
अब हल्कू को कंबल के अभाव मे पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़कर ही पूस की हड्डी कँपा देनेवाली ठंडी रात में अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है | उसके साथ उसका कुत्ता भी है | ठंड जब असहनीय हो जाती है, तो हल्कू मानवता और पशु के बीच का भेद भूलकर, जबरा को अपनी गोद में चिपका लेता है |
रात के तीसरे पहर, जबरा किसी जानवर की आहट पाकर ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगता है और खेत की ओर भागता है | अब हल्कू को स्पष्ट पता चल जाता है कि नीलगायों का एक झुंड खेत में चर रहा है और फसल नष्ट हो रही है फिर भी वह भयंकर ठंड और आलस्य के कारण कंबल मे ही जमा रहता है | ठंड से बचने के लिए वह पत्तियों को जलाता है | आग की गर्मी से उसे क्षणिक सुख मिलता है और वह आलस्य के बंधन में जकड़कर वहीं गर्म राख के पास चादर ओढ़कर सो जाता है और उधर नीलगायें रातभर फसल का सफाया करती रहती हैं | हल्कू को खेत के उजड़ जाने का कोई दुःख नहीं है बल्कि वह खुश है कि अब उसे पूस की ठंडी रातों में खेत पर नहीं सोना पड़ेगा |
अब वह मजदूरी करके पेट पालेगा, जिसमें कम से कम उसे रात की इस असहनीय ठंड से छुटकारा तो मिल जाएगा | कहानी भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता और ज़मींदारी-साहूकारी व्यवस्था द्वारा किए गए उनके शोषण को उजागर करती है | साहूकार उससे कंबल के पैसे नहीं लेता तो आज उसकी मनोदशा ऐसे नहीं होती |
हल्कू का अपनी फसल नष्ट हो जाने पर खुश होना, किसान की उस मानसिकता को दर्शाता है, जहाँ अत्यधिक शोषण और कष्ट के कारण वह अपनी किसानी छोड़कर मजदूरी करने को भी बेहतर विकल्प मानने लगता है |
तीसरी कहानी है – ठाकुर का कुआँ कहानी का सारांश |
‘ठाकुर का कुआँ’ मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत संवेदनशील और यथार्थवादी कहानी है, जो भारतीय समाज में व्याप्त भयंकर छुआछूत याने अस्पृश्यता और जातिगत उत्पीड़न की समस्या को उजागर करती है | यह कहानी 1932 में प्रकाशित हुई थी |
गंगी अछूत जाति की एक साहसी और समझदार स्त्री है | उसका पती जोखू , बीमार है और प्यास से तड़प रहा है | जोखू जैसे ही लोटा मुँह से लगाता है, तो पानी में सख्त बदबू आती है | पता चलता है कि उनके घर के पास स्थित कुएँ का पानी गंदा हो गया है | यह पानी पीने से जोखू की बीमारी और बढ़ सकती है | अछूत होने के कारण, जोखू और गंगी गाँव के सवर्णों के कुओं से पानी नहीं भर सकते | गाँव में सिर्फ ठाकुर का कुआँ और साहू का कुआँ ही है, जिनका पानी साफ है, लेकिन इन पर उनका एकाधिकार है और सख्त पहरा है |
बीमार पति की प्यास बुझाने और उसे गंदा पानी पीने से रोकने के लिए, गंगी रात के अंधेरे में चुपचाप ठाकुर के कुएँ से पानी लाने का निश्चय करती है | कुए के पहरे पर बैठे लोगों की बातों से गंगी को पता चलता है की ऊँची जाति के लोग चोर, झूठे , मक्कार , फरेबी और शोषक होते हुए भी समाज में ऊंचा स्थान पाते है जबकि गंगी और उसके जाती के लोग ईमानदारी से मज़दूरी करके भी ‘नीच’ माने जाते हैं | गंगी का विद्रोही मन इन सामाजिक पाबंदियों से तिलमिला जाता है |
ठाकुर के कुएं का पानी गंगी के लिए आज के दिन मे किसी अमृत से कम नहीं | वह उसे लेने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है | क्योंकि घड़ा पानी मे गिरने के साथ ही आवाज होती है और ठाकुर आवाज लगा देता है |
गंगी घबराहट में रस्सी छोड़कर कुएँ की जगत से कूदकर भाग खड़ी होती है | उसे डर है कि यदि वह पकड़ी गई, तो उसे मार – मारकर अधमरा कर दिया जाएगा | घर जाने के बाद जोखू उसे वही गंदा पानी पीते हुए दिखता है |
गंगी की सारी मेहनत, साहस और संघर्ष व्यर्थ चला जाता है | दलित दंपति को साफ पानी जैसा बुनियादी मानवाधिकार भी इस क्रूर सामाजिक व्यवस्था के कारण नहीं मिल पाता | यह कहानी भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई …. “छुआछूत” को केंद्र में रखकर दलित वर्ग की त्रासदी को लेकर लिखी गई है |
‘पानी’ यहाँ जीवन, समानता और बुनियादी मानवाधिकारों का प्रतीक है | कहानी दिखाती है कि कैसे दलितों को जीवन के लिए आवश्यक जल जैसे स्रोत से भी वंचित रखा जाता था |
गंगी का चरित्र उस दलित स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी सामाजिक विवशता के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस तो करती है, लेकिन अंत में सामाजिक जकड़न के कारण हार मानकर लौट आती है |
कहानी में ठाकुरों और साहूकारों के अपराधिक, भ्रष्ट और अनैतिक व्यवहार का चित्रण किया गया है | लेखक दिखाते है कि चोरी करनेवाले और रिश्वत देनेवाले लोग समाज में ऊंचा स्थान पाते है जबकि मेहनती और गरीब लोग ‘नीचा’ |
चौथी कहानी है – ‘गुल्ली-डंडा’ | कहानी का सारांश |
बचपन की मासूमियत और बड़े होने पर सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण मनुष्य के संबंधों में आए बदलावों को दर्शाने वाली एक मार्मिक कहानी है | यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है |
कथानायक कहानी की शुरुआत में गुल्ली-डंडा खेल की प्रशंसा करता है | वह इसे ‘सब खेलों का राजा’ कहता है, क्योंकि यह बिना किसी खर्च, बिना किसी उपकरण के आसानी से खेला जा सकता है, जबकि अंग्रेज़ी खेलों में बहुत पैसा व्यय होता है | वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब खेल में अमीरी-गरीबी, जात-पात या पद-प्रतिष्ठा का कोई भेद नहीं था |
इन्ही दिनों की याद करते हुए वह अपने बालसखा “गया” को याद करता है जो गुल्ली-डंडा का माहिर खिलाड़ी था | गया अपने दाँव के लिए कठोर रहता था और कथानायक जो अभी इंजीनियर बन चुका है , के चोरी करने या बेईमानी करने पर उसे डाँटता भी था, लेकिन उन दोनों के बीच निर्मल दोस्ती थी |
लगभग 20-25 साल बाद, कथानायक एक इंजीनियर के रूप मे अपने पुराने कसबे के डाक बंगले में आता है | उसे अपने बचपन के दिन और गुल्ली-डंडे का खेल याद आता है | वह गया को खोजता है | गया अब मजदूर है जिसे साईस कहा जाता है जो घोड़ों की देखरेख करता है |
इस कहानी का नायक , गया से मिलकर उसके साथ गुल्ली-डंडा खेलने का आग्रह करता है, ताकि वह अपने बचपन के दिनों को फिर से जी सके | जब वे खेलते हैं, तो इंजीनियर को आश्चर्य होता है कि गया बहुत कमज़ोर खेल रहा है |
वह न तो ठीक से गुल्ली उछाल पाता है, न डंडे को छू पाता है | इंजीनियर जान-बूझकर कई बार बेईमानी भी करता है, पर गया उसे टोकता नहीं, न ही विरोध करता है, बल्कि चुपचाप उसकी धाँधली सहता रहता है |
अगले दिन, इंजीनियर साहब गया को उसके बराबरी के लड़कों के साथ गुल्ली-डंडा खेलते हुए देखते है | वह देखते है की गया उन्हें जबरदस्त पिटा रहा है और तनिक भी बेईमानी या ढील नहीं दे रहा है | इससे आप ने क्या निष्कर्ष निकाला | यही ना , की गया ने कल उसके साथ केवल औपचारिकता निभाई थी और दया के कारण उसे जीतने दिया था | क्योंकि अब वह समझता है कि पद और प्रतिष्ठा की दीवार ने उन दोनों के बीच बचपन के निश्छल प्रेम और समानता को खत्म कर दिया है |
इंजीनियर , इस कथा का नायक महसूस करता है कि गया आज भी खेल का चैंपियन है, लेकिन उनका बचपन का सच्चा, बराबरी का रिश्ता अब हमेशा के लिए खो चुका है | उसकी जगह अफ़सर और मजदूर के औपचारिक और सम्मान-भरे संबंध ने ले ली है | पद और प्रतिष्ठा के कारण मनुष्य के स्वाभाविक और निश्छल संबंध नष्ट हो जाते है | लेखक प्रेमचंद दिखाते है कि बचपन में गरीबी-अमीरी, जात-पात, और पद का कोई भेद नहीं होता, और खेल में भी सभी समान होते हैं |
प्रेमचंदजी की हर एक कहानी कुछ न कुछ सीख लिए जरूर होती है | उनके विषय तब भी समाज मे मौजूद थे और आज भी है | इसीलिये उनकी कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है और इसीलिए शायद लेखक आज भी “उपन्यास सम्राट” के पद पर आसीन है | इसीलिए “सारांश बुक ब्लॉग” के माध्यम से हम उनके उपन्यासों को आप तक पहुचाने की कोशिश कर रहे है | इसीलिए “सारांश बुक ब्लॉग” के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए | तब तक पढ़ते रहिए | अमेजन से अभी खरीदे और पढ़ना शुरू करे | खुशहाल रहिए | मिलते है और एक नई किताब के साथ तब तक के लिए ….
धन्यवाद !!
Check out PREMA on our youtube channel
” FAQ सेक्शन में आपका स्वागत है |
सवाल है ? जवाब यहाँ है | (FAQs SECTION)
Q1. मानसरोवर इस प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है ?
A. मानसरोवर इस प्रसिद्ध किताब के लेखक मुंशी प्रेमचंद है है |
Q2. मानसरोवर इस प्रसिद्ध किताब मे कुल कितनी कहानियाँ है ?
A. मानसरोवर इस प्रसिद्ध किताब मे कुल 23 कहानियाँ है |
Q.3.मानसरोवर इस प्रसिद्ध किताब के कुल कितने भाग प्रकाशित हो चुके है ?
A. मानसरोवर इस प्रसिद्ध किताब के कुल आठ भाग प्रकाशित हो चुके है |
Q.5.मानसरोवर के कवि कौन है ?
A.पहली बात तो यह की मानसरोवर कविताओ का नहीं कहानियों का संग्रह है जो गद्य का भाग है |